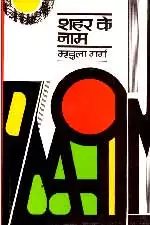|
कहानी संग्रह >> शहर के नाम शहर के नाममृदुला गर्ग
|
232 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है शहर के नाम कहानी संग्रह...
Shahar ke nam
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
व्यक्ति समाज में ही नहीं जीता, समाज को भी जीता है। एक की पीड़ा दूसरे की बनी तभी मानवीय संवेदना जन्म लेती है। फिर समाज केवल नारी और पुरुष का समूह ही नहीं होता वरन् गाँव, देश, शहर व सारा का सारा परिवेश भी उसमें अभिन्न अंग होता है। इस संग्रह की कहानियों रिश्तों और संवेदनाओं से रंगी हुई हैं। इनके पात्र बाहरी जन नहीं बने रहते। शहर के साथ उनका संबंध अनेक रंगों में खिलता है, फूलता-फलता और मुरझाता है और हर हाल में पाठक को बाध्य करता है कि वह जो घट चुका, उसके आगे बार-बार चिन्तन करे।
हर साँस के साथ
अपनी सृजन-प्रक्रिया के बारे में बात करने से मैं कतराती रही हूँ। मुझे लगता है यह प्रक्रिया मेरे जन्म से शुरू होकर अब तक निरन्तर चली आ रही है, इसलिए इसे मैं कुछ एक क्षणों के बीच बाँधकर, सृजन-प्रक्रिया की संज्ञा नहीं दे सकती। फिर भी इस जीवन-व्यापी प्रक्रिया को जानना जरूरी है, रचना के आधार को समझने के लिए। सबसे ज्यादा शायद खुद मेरे लिए। इतना मैं जानती हूँ कि आये दिन मैं उत्कट अनुभवों से गुज़रती हूँ और उनसे उत्पन्न सृजन-प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। पर अनुभूति, कृति में कैसे बदलती है, यह जानने का प्रयास भी कर देखें।
मेरे लिए उत्कट अनुभव, कृति का आधार केवल उसी तरह है, जिस तरह वृक्ष का आधार बीज माना जा सकता है। बीज को यदि उर्वर भूमि न मिले, सूर्य का प्रकाश और जल उपलब्ध न हो वह सदा-सदा के लिए सूखा बीज बना पड़ा रहेगा। उसी प्रकार अनुभव को मानवीय अन्तरात्मा की भूमि न मिले, संवेदनात्मक ज्ञान का जल न सींचे और सबसे बढ़कर कल्पना के सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक न बने तो गीले कपड़े में बँधी मूँग की तरह, वह अंकुरित तो हो जाएगा पर दो-चार दिन के अन्दर सड़ जाएगा। पौधे की तरह विकसित नहीं होगा। यूँ तो जीवन मैं सैकड़ों अनुभव होते हैं पर कहानी या उपन्यास का आधार कुछ ही बन पाते हैं। ज़्यादातर समय के साथ धुँधले पड़ते जाते हैं और कालान्तर में हम उन्हें भूल जाते हैं। या वे मात्र घटनाएँ बनकर हमारी स्मृति में शेष रहते हैं। ऐसे अनुभवों को हम किस्सों की तरह सुना सकते हैं और उनसे कहानी या उपन्यास का प्रस्फुटन नहीं कर सकते। पर कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं, जो केवल घटना बनकर नहीं घटते। अपने पर्यावरण के पूरे रंग, रूप, गंध, स्वर सहित हमारी चेतना में प्रवेश पाते हैं। समय के साथ धुँधले पड़ने के बजाय अधिक समृद्ध होते रहते हैं। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, नितान्त वैयक्तिक और असंगत अनुभव भी निर्वैयक्तिक और सोद्देश्य बन सकता है।
अनुभव को समृद्ध बनाने में तीन मूल संवेदन शक्तियाँ काम करती हैं। पहली है स्मृति। विगत में हुए अनुभवों की स्मृति नये अनुभव से मिलती है। अनुभूति की सीमा रेखा कहीं सिकुड़ती है तो कहीं फैल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, मानव एक अद्भुत संग्रहालय है। उसमें अनेकानेक ऐसे तथ्य समाहित रहते हैं जिनका हम सचेत रूप से पुन: स्मरण नहीं करते। बचपन के जिस काल को हम ‘होश सँभालने के पहले’ की संज्ञा देते हैं, उनकी अनेक सूक्ष्म और तीव्र अनुभूतियाँ हमारे स्मृति संग्रहालय में संचित रहती हैं। शायद ‘होश सँभालने के बाद’ का उत्कट-से-उत्कट अनुभव भी चेतन मन की अर्धविस्मृति, पर अवचेतन की जीवन्त स्मृतियों की पीड़ा को स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, उनसे समृद्ध होकर नयी पीड़ा को जन्म अवश्य देता है। जहाँ स्मृति का मन्थन मूल अनुभव का रूप इतना विकसित कर देता है कि वह अपनी व्यापकता में सर्वथा भिन्न या न पहचानने योग्य बन जाता है, यानी स्मृति में परिमार्जित अनुभूति, मूल अनुभव से अधिक उत्कट प्रतीत होने लगती है; वहाँ मेरे लिए उपन्यास का सूत्रपात होता है। इसके विपरीत जब स्मृति से छनकर आने पर भी, अनुभव अपने मूल रूप में अधिक उत्कट और पारदर्शी बना रहता है, वह कहानी का रूप ले लेता है।
हो सकता हैं औरों का अनुभव इससे भिन्न हो।
स्मृति के साथ दूसरी संवेदन शक्ति, जो मुझे स्पन्दित करती है, वह है, कल्पना। घटित को जब-जब मैं पुन: स्मरण करती हूँ, उसके रंग-रूप-स्वर-गन्ध को कल्पना नये-नये रस-रंग-आकार से पूरित करती चलती है। मैं अनुभव को ‘जो घटा’ के रूप में न याद रखकर, ‘जो घट सकता था’ के रूप में याद करने लगती हूं। सृजनशील कल्पना तो रचनाकार का स्वभावगत धर्म है। उसी से सौन्दर्य की अनुभूति होती है और रचनाकार का अनुभव वैयक्तिक न रहकर सार्वभौमिक बन जाता है। पाठक उसमें सम्मिलित हो जाता है। अर्थात् कल्पना वह उत्प्रेरक है, जो कृतिकार के वैयक्तिक और साधारण अनुभव को सौन्दर्य के अनुभव का वाहक बना देती है। और जाहिर है कि उसके बगैर कृति का जन्म संभव नहीं है।
तीसरी शक्ति है वांछा। यहाँ अनुभव में एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। अब मैं उसे केवल ‘जो घट सकता था’ के रूप में नहीं देखती, बल्कि उससे आगे बढ़कर ‘जो घटना चाहिए’ के रूप में देखने लगती हूँ। अपने सम्पूर्ण जीवनकाल के अनुभव, अध्ययन, भावात्मक संवेदना और बौद्धिक आकलन द्वारा, हम एक निजी या विशिष्ट जीवन दृष्टि अर्जित करते हैं। हर नये अनुभव को भोग लेने पर, हम इसी जीवन-दृष्टि से उसे देखते-परखते और आत्मसात करते हैं। कल्पना द्वारा समृद्ध अनुभव और पूर्वसंचित जीवन-दृष्टि की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से हमारे मानस में एक नये वांछित संसार की संरचना होती है। जो जीवन के समानान्तर तो चलता है पर उसकी सीमा-बिन्दुओं के बीच बँधा नहीं रहता। अपनी यात्रा में उससे बहुत आगे निकल जाता है। वास्तविक संसार अपने देश काल के यथार्थ की परिधि में बँधा रहता है। रचना संसार इस यथार्थ को अपने में समाहित कर लेने के बाद, इन परिधियों को लाँघ जाता है। और एक नहीं अनेक दिशाओं में विस्तीर्ण होता है। इस प्रकार जब वास्तविक अनुभव वांछित अनुभव में परिवर्तित हो जाता है तो मेरे लिए साहित्यिक कृति को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया आरम्भ होती है।
इस प्रक्रिया में जो था, जो है, जो हो सकता है और जो होना चाहिए, चारों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है। जैसे ही वांछित अनुभव को शब्दबद्ध करना आरम्भ करती हूँ, मेरे जीवन और जीवन-दृष्टि से उत्पन्न अनेक पात्र लेखिनी से शब्द छीन, अपनी जीवन लीला शुरू कर देते हैं।
प्रत्येक पात्र के विकास का एक स्वभावगत तर्क होता है, जो उसकी गति और दिशा को निर्धारित करता है। यह तर्क उसे मेरी भावात्मक संवेदना और जीवन-दृष्टि के समन्वय से बनी मानवीय चेतना से प्राप्त होता है। पर वह बौद्धिक न होकर पराबौद्धिक होता है।
ऐसा नहीं हैं कि लेखक का कोई उद्देश्य नहीं होता। बल्कि कहें तो उद्देश्यहीन व्यक्ति सृजनशील हो ही नहीं सकता। अनुभव को पूरे पर्यावरण के संदर्भ में, उत्कटता से वही व्यक्ति सम्प्रेषित कर सकता है जो अपने देश के विरोधाभासों की तीव्रता से महसूस करता हो। और ऐसा व्यक्ति ही सतत सृजनशील व्यक्ति के कल्पनाप्रवण धर्म का निर्वाह कर सकता है। क्योंकि वह स्वभावगत रूप से वांछित संसार की परिकल्पना और संरचना के लिए बाध्य महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई महत् उद्देश्य होगा ही। यह दूसरी बात है कि उसका संबंध उसके पूरे व्यक्तित्व और जीवन से होगा, केवल उस कृति से नहीं, जो उस समय शब्दबद्ध हो रही है।
मुक्तिबोध ने कहा था, ‘‘आज ता लेखक अनुभूत यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियाँ और उपन्यास गढ़ना चाहता है, उसमें मानवीय अन्तरात्मा की हलचल मचाने वाली पीड़ा के अभाव में, लेखक यदि अनुभूत का सहारा लेकर भी उपन्यास या कहानी गढ़ेगा, तो वह एकांगी और असत्य होगी, क्योंकि वह अनुभव की अनुकृति भर होगी, सृजनात्मक कृति नहीं। अनुभव को संवेदना के स्तर पर सार्वजनीन बनाने के बजाय व्यक्तिनिष्ठ बना देगी, जो पाठक के भावबोध का हिस्सा कभी नहीं बन सकेगी।
कोई भी ईमानदार लेखक इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जाने-अनजाने, संस्कारवश, वह कुछेक अनुभवों को ही सृजनशीलता का आधार बनाता है। संस्कारवश ही, वह कभी-कभी अधिक व्यापक या सार्वजनिक रूप से अर्थपूर्ण अनुभवों को छोड़ देता है। इसलिए लेखक का अनुभव, वास्तव में एकांगी ही नहीं, अधूरा सच या अविश्वसनीय भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने साबित करके दिखला दिया है कि एक ही घटना का वर्णन, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से करते हैं। आँखों देखी घटना के जब एक से ज़्यादा विवरण हो सकते हैं तो अलग-अलग समय पर, एक जैसे अनुभवों से गुजरने वालों का विवरण तो एकदम भिन्न हो ही सकता है। हम वही देखते या अनुभव करते हैं, जो हमारा नजरिया या दृष्टिकोण हमें महसूस करवाता है। केवल इसलिए किसी अनुभूति को पूर्णतया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि वह लिखने वाले का अपना भोगा हुआ यथार्थ है। सवाल दरअसल यह नहीं है कि इस उपन्यास का आधार किस अनुभव को बनाते हैं, बल्कि यह कि उसका रोपण किस मानवीय चेतना या संवेदात्मक भावभूमि में करते हैं। हमारी कल्पना की दिशा क्या है ? सार्वजनिक या सामाजिक पीड़ा को हम कहाँ तक अपनी अन्तरात्मा की पीड़ा की तरह महसूस करते हैं और अपने जीवन और व्यक्तित्व से अन्नत: हम चाहते क्या हैं ?
जिन लोगों के व्यक्तित्व और जीवन का उद्देश्य पद, सम्पदा, सामाजिक मान-मर्यादा प्राप्त करना है, वे कितने भी प्रगतिवादी या समाजवादी दावे क्यों न कर लें, अपने या किसी और के कितने भी पीड़ा दायक अनुभवों का चयन क्यों न कर डालें, अपने पात्रों को सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि बनाकर ही दम लें, फिर भी उनके उपन्यास का मूल स्वर या संवेदना उपभोक्ता संस्कृति या महाजनी सभ्यता की महत्त्वाकांक्षाओं की रहेगी। इसके विपरीत यदि उनकी मानवीय अन्तरात्मा अभी जीवित है, और समाज के आमूल परिवर्तन में सक्रिय भाग लेना चाहते हैं, तो उनके पात्र चाहे जिस वर्ग से आएँ, कहानी का स्वर या संवेदना, समाजनिष्ठ होगी। दूसरे शब्दों में, एक तरफ़ जहाँ संभव है कि हमारी मानवीय संवेदना दूसरों की पीड़ा को हमारा अपना अनुभव बना दे, वहाँ यह भी सहज संभव है कि इस संवेदना के अभाव में, हमारे अपने अनुभव किसी दूसरे के न बन पाये।
जो लेखक उपन्यास या कहानी को सामाजिक विचारधारा की तरह देखता है, उसे अपनी निजी तृष्णा-वितृष्णा या विवेक-पीड़ा का अंग नहीं बनाता, वह राजनीतिक मसविदा तो लिख सकता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन भी कर सकता है, नसीहत दे सकता है, और संभवत: सामाजिक क्रान्ति की रूपरेखा भी तैयार कर सकता हो, पर न तो वह उसमें सक्रिय भाग ले सकता है न उस सृजनात्मक संसार की संरचना कर सकता है, जिसे हम उपन्यास, कहानी, नाटक या काव्य के नाम से पुकारते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि वह वैयक्तिक आवेग के साथ उसे महसूस करे और अपनी विशिष्ट जीवन-दृष्टि से उनका मूल्यांकन करे। यह दूसरी बात है कि आप राजनीतिक मसविदे या समाजशास्त्रीय अध्ययन को साहित्य-सृजन से अधिक महत्त्वपूर्ण मानें।
ऐसा कोई दावा मेरा नहीं है कि साहित्य-सृजन, जीवन के अन्य कर्मो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण या उदात्त है। पर जो भी वह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सृजन-प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रकार की स्वभावगत क्रिया है, जिससे सृजनशील व्यक्ति चाहकर भी त्राण नहीं पा सकता। मैंने पाया कि मैं पूरी सृजन-प्रक्रिया के दौरान विरोधी मन:स्थितियों के बीच खिंचती रहती हूँ। एक ओर अपनी सारी मानवीय पीड़ा और तृष्णा-वितृष्णा को शब्द देना चाहती हूँ, तो दूसरी तरफ़ जो अत्यन्त वैयक्तिक और निजी है, उसे दूसरों की नजरों से बचाये रखना चाहती हूँ। अन्तत: द्वन्द्व में, मेरे व्यक्ति के ऊपर सर्जक की जीत होती है तभी कृति पाठक के सम्मुख आ पाती है।
मेरे लिए उत्कट अनुभव, कृति का आधार केवल उसी तरह है, जिस तरह वृक्ष का आधार बीज माना जा सकता है। बीज को यदि उर्वर भूमि न मिले, सूर्य का प्रकाश और जल उपलब्ध न हो वह सदा-सदा के लिए सूखा बीज बना पड़ा रहेगा। उसी प्रकार अनुभव को मानवीय अन्तरात्मा की भूमि न मिले, संवेदनात्मक ज्ञान का जल न सींचे और सबसे बढ़कर कल्पना के सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक न बने तो गीले कपड़े में बँधी मूँग की तरह, वह अंकुरित तो हो जाएगा पर दो-चार दिन के अन्दर सड़ जाएगा। पौधे की तरह विकसित नहीं होगा। यूँ तो जीवन मैं सैकड़ों अनुभव होते हैं पर कहानी या उपन्यास का आधार कुछ ही बन पाते हैं। ज़्यादातर समय के साथ धुँधले पड़ते जाते हैं और कालान्तर में हम उन्हें भूल जाते हैं। या वे मात्र घटनाएँ बनकर हमारी स्मृति में शेष रहते हैं। ऐसे अनुभवों को हम किस्सों की तरह सुना सकते हैं और उनसे कहानी या उपन्यास का प्रस्फुटन नहीं कर सकते। पर कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं, जो केवल घटना बनकर नहीं घटते। अपने पर्यावरण के पूरे रंग, रूप, गंध, स्वर सहित हमारी चेतना में प्रवेश पाते हैं। समय के साथ धुँधले पड़ने के बजाय अधिक समृद्ध होते रहते हैं। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, नितान्त वैयक्तिक और असंगत अनुभव भी निर्वैयक्तिक और सोद्देश्य बन सकता है।
अनुभव को समृद्ध बनाने में तीन मूल संवेदन शक्तियाँ काम करती हैं। पहली है स्मृति। विगत में हुए अनुभवों की स्मृति नये अनुभव से मिलती है। अनुभूति की सीमा रेखा कहीं सिकुड़ती है तो कहीं फैल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, मानव एक अद्भुत संग्रहालय है। उसमें अनेकानेक ऐसे तथ्य समाहित रहते हैं जिनका हम सचेत रूप से पुन: स्मरण नहीं करते। बचपन के जिस काल को हम ‘होश सँभालने के पहले’ की संज्ञा देते हैं, उनकी अनेक सूक्ष्म और तीव्र अनुभूतियाँ हमारे स्मृति संग्रहालय में संचित रहती हैं। शायद ‘होश सँभालने के बाद’ का उत्कट-से-उत्कट अनुभव भी चेतन मन की अर्धविस्मृति, पर अवचेतन की जीवन्त स्मृतियों की पीड़ा को स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, उनसे समृद्ध होकर नयी पीड़ा को जन्म अवश्य देता है। जहाँ स्मृति का मन्थन मूल अनुभव का रूप इतना विकसित कर देता है कि वह अपनी व्यापकता में सर्वथा भिन्न या न पहचानने योग्य बन जाता है, यानी स्मृति में परिमार्जित अनुभूति, मूल अनुभव से अधिक उत्कट प्रतीत होने लगती है; वहाँ मेरे लिए उपन्यास का सूत्रपात होता है। इसके विपरीत जब स्मृति से छनकर आने पर भी, अनुभव अपने मूल रूप में अधिक उत्कट और पारदर्शी बना रहता है, वह कहानी का रूप ले लेता है।
हो सकता हैं औरों का अनुभव इससे भिन्न हो।
स्मृति के साथ दूसरी संवेदन शक्ति, जो मुझे स्पन्दित करती है, वह है, कल्पना। घटित को जब-जब मैं पुन: स्मरण करती हूँ, उसके रंग-रूप-स्वर-गन्ध को कल्पना नये-नये रस-रंग-आकार से पूरित करती चलती है। मैं अनुभव को ‘जो घटा’ के रूप में न याद रखकर, ‘जो घट सकता था’ के रूप में याद करने लगती हूं। सृजनशील कल्पना तो रचनाकार का स्वभावगत धर्म है। उसी से सौन्दर्य की अनुभूति होती है और रचनाकार का अनुभव वैयक्तिक न रहकर सार्वभौमिक बन जाता है। पाठक उसमें सम्मिलित हो जाता है। अर्थात् कल्पना वह उत्प्रेरक है, जो कृतिकार के वैयक्तिक और साधारण अनुभव को सौन्दर्य के अनुभव का वाहक बना देती है। और जाहिर है कि उसके बगैर कृति का जन्म संभव नहीं है।
तीसरी शक्ति है वांछा। यहाँ अनुभव में एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। अब मैं उसे केवल ‘जो घट सकता था’ के रूप में नहीं देखती, बल्कि उससे आगे बढ़कर ‘जो घटना चाहिए’ के रूप में देखने लगती हूँ। अपने सम्पूर्ण जीवनकाल के अनुभव, अध्ययन, भावात्मक संवेदना और बौद्धिक आकलन द्वारा, हम एक निजी या विशिष्ट जीवन दृष्टि अर्जित करते हैं। हर नये अनुभव को भोग लेने पर, हम इसी जीवन-दृष्टि से उसे देखते-परखते और आत्मसात करते हैं। कल्पना द्वारा समृद्ध अनुभव और पूर्वसंचित जीवन-दृष्टि की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से हमारे मानस में एक नये वांछित संसार की संरचना होती है। जो जीवन के समानान्तर तो चलता है पर उसकी सीमा-बिन्दुओं के बीच बँधा नहीं रहता। अपनी यात्रा में उससे बहुत आगे निकल जाता है। वास्तविक संसार अपने देश काल के यथार्थ की परिधि में बँधा रहता है। रचना संसार इस यथार्थ को अपने में समाहित कर लेने के बाद, इन परिधियों को लाँघ जाता है। और एक नहीं अनेक दिशाओं में विस्तीर्ण होता है। इस प्रकार जब वास्तविक अनुभव वांछित अनुभव में परिवर्तित हो जाता है तो मेरे लिए साहित्यिक कृति को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया आरम्भ होती है।
इस प्रक्रिया में जो था, जो है, जो हो सकता है और जो होना चाहिए, चारों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है। जैसे ही वांछित अनुभव को शब्दबद्ध करना आरम्भ करती हूँ, मेरे जीवन और जीवन-दृष्टि से उत्पन्न अनेक पात्र लेखिनी से शब्द छीन, अपनी जीवन लीला शुरू कर देते हैं।
प्रत्येक पात्र के विकास का एक स्वभावगत तर्क होता है, जो उसकी गति और दिशा को निर्धारित करता है। यह तर्क उसे मेरी भावात्मक संवेदना और जीवन-दृष्टि के समन्वय से बनी मानवीय चेतना से प्राप्त होता है। पर वह बौद्धिक न होकर पराबौद्धिक होता है।
ऐसा नहीं हैं कि लेखक का कोई उद्देश्य नहीं होता। बल्कि कहें तो उद्देश्यहीन व्यक्ति सृजनशील हो ही नहीं सकता। अनुभव को पूरे पर्यावरण के संदर्भ में, उत्कटता से वही व्यक्ति सम्प्रेषित कर सकता है जो अपने देश के विरोधाभासों की तीव्रता से महसूस करता हो। और ऐसा व्यक्ति ही सतत सृजनशील व्यक्ति के कल्पनाप्रवण धर्म का निर्वाह कर सकता है। क्योंकि वह स्वभावगत रूप से वांछित संसार की परिकल्पना और संरचना के लिए बाध्य महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई महत् उद्देश्य होगा ही। यह दूसरी बात है कि उसका संबंध उसके पूरे व्यक्तित्व और जीवन से होगा, केवल उस कृति से नहीं, जो उस समय शब्दबद्ध हो रही है।
मुक्तिबोध ने कहा था, ‘‘आज ता लेखक अनुभूत यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियाँ और उपन्यास गढ़ना चाहता है, उसमें मानवीय अन्तरात्मा की हलचल मचाने वाली पीड़ा के अभाव में, लेखक यदि अनुभूत का सहारा लेकर भी उपन्यास या कहानी गढ़ेगा, तो वह एकांगी और असत्य होगी, क्योंकि वह अनुभव की अनुकृति भर होगी, सृजनात्मक कृति नहीं। अनुभव को संवेदना के स्तर पर सार्वजनीन बनाने के बजाय व्यक्तिनिष्ठ बना देगी, जो पाठक के भावबोध का हिस्सा कभी नहीं बन सकेगी।
कोई भी ईमानदार लेखक इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जाने-अनजाने, संस्कारवश, वह कुछेक अनुभवों को ही सृजनशीलता का आधार बनाता है। संस्कारवश ही, वह कभी-कभी अधिक व्यापक या सार्वजनिक रूप से अर्थपूर्ण अनुभवों को छोड़ देता है। इसलिए लेखक का अनुभव, वास्तव में एकांगी ही नहीं, अधूरा सच या अविश्वसनीय भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने साबित करके दिखला दिया है कि एक ही घटना का वर्णन, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से करते हैं। आँखों देखी घटना के जब एक से ज़्यादा विवरण हो सकते हैं तो अलग-अलग समय पर, एक जैसे अनुभवों से गुजरने वालों का विवरण तो एकदम भिन्न हो ही सकता है। हम वही देखते या अनुभव करते हैं, जो हमारा नजरिया या दृष्टिकोण हमें महसूस करवाता है। केवल इसलिए किसी अनुभूति को पूर्णतया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि वह लिखने वाले का अपना भोगा हुआ यथार्थ है। सवाल दरअसल यह नहीं है कि इस उपन्यास का आधार किस अनुभव को बनाते हैं, बल्कि यह कि उसका रोपण किस मानवीय चेतना या संवेदात्मक भावभूमि में करते हैं। हमारी कल्पना की दिशा क्या है ? सार्वजनिक या सामाजिक पीड़ा को हम कहाँ तक अपनी अन्तरात्मा की पीड़ा की तरह महसूस करते हैं और अपने जीवन और व्यक्तित्व से अन्नत: हम चाहते क्या हैं ?
जिन लोगों के व्यक्तित्व और जीवन का उद्देश्य पद, सम्पदा, सामाजिक मान-मर्यादा प्राप्त करना है, वे कितने भी प्रगतिवादी या समाजवादी दावे क्यों न कर लें, अपने या किसी और के कितने भी पीड़ा दायक अनुभवों का चयन क्यों न कर डालें, अपने पात्रों को सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि बनाकर ही दम लें, फिर भी उनके उपन्यास का मूल स्वर या संवेदना उपभोक्ता संस्कृति या महाजनी सभ्यता की महत्त्वाकांक्षाओं की रहेगी। इसके विपरीत यदि उनकी मानवीय अन्तरात्मा अभी जीवित है, और समाज के आमूल परिवर्तन में सक्रिय भाग लेना चाहते हैं, तो उनके पात्र चाहे जिस वर्ग से आएँ, कहानी का स्वर या संवेदना, समाजनिष्ठ होगी। दूसरे शब्दों में, एक तरफ़ जहाँ संभव है कि हमारी मानवीय संवेदना दूसरों की पीड़ा को हमारा अपना अनुभव बना दे, वहाँ यह भी सहज संभव है कि इस संवेदना के अभाव में, हमारे अपने अनुभव किसी दूसरे के न बन पाये।
जो लेखक उपन्यास या कहानी को सामाजिक विचारधारा की तरह देखता है, उसे अपनी निजी तृष्णा-वितृष्णा या विवेक-पीड़ा का अंग नहीं बनाता, वह राजनीतिक मसविदा तो लिख सकता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन भी कर सकता है, नसीहत दे सकता है, और संभवत: सामाजिक क्रान्ति की रूपरेखा भी तैयार कर सकता हो, पर न तो वह उसमें सक्रिय भाग ले सकता है न उस सृजनात्मक संसार की संरचना कर सकता है, जिसे हम उपन्यास, कहानी, नाटक या काव्य के नाम से पुकारते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि वह वैयक्तिक आवेग के साथ उसे महसूस करे और अपनी विशिष्ट जीवन-दृष्टि से उनका मूल्यांकन करे। यह दूसरी बात है कि आप राजनीतिक मसविदे या समाजशास्त्रीय अध्ययन को साहित्य-सृजन से अधिक महत्त्वपूर्ण मानें।
ऐसा कोई दावा मेरा नहीं है कि साहित्य-सृजन, जीवन के अन्य कर्मो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण या उदात्त है। पर जो भी वह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सृजन-प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रकार की स्वभावगत क्रिया है, जिससे सृजनशील व्यक्ति चाहकर भी त्राण नहीं पा सकता। मैंने पाया कि मैं पूरी सृजन-प्रक्रिया के दौरान विरोधी मन:स्थितियों के बीच खिंचती रहती हूँ। एक ओर अपनी सारी मानवीय पीड़ा और तृष्णा-वितृष्णा को शब्द देना चाहती हूँ, तो दूसरी तरफ़ जो अत्यन्त वैयक्तिक और निजी है, उसे दूसरों की नजरों से बचाये रखना चाहती हूँ। अन्तत: द्वन्द्व में, मेरे व्यक्ति के ऊपर सर्जक की जीत होती है तभी कृति पाठक के सम्मुख आ पाती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i